By Suresh Agrawal, Kesinga, Odisha
 यूँ तो लम्बे समय से कालाहाण्डी का नाम देश के सर्वाधिक पिछड़े ज़िले के रूप में शामिल रहा है, परन्तु अब यहाँ की फ़िज़ा काफी बदल चुकी है,आवश्यकता है तो बस उसे तराशने एवं सहेज कर रखने की। हाल ही के एक आंकलन में कालाहाण्डी को देश के अठारह महत्वाकांक्षी ज़िलों में से एक बतलाया गया है। जानकारी के मुताबिक़ ज़िले में केवल धान एवं कपास का ही सालाना उत्पादन कोई 16 करोड़ का होता है, जबकि फल एवं सब्जियों से भी कोई पांच करोड़ की आय होती है। सूचनानुसार इससे राज्य सरकार को भी 53 करोड़ का शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। यह सब प्रकृति प्रदत्त अथवा परम्परागत खेती से प्राप्त होता है, परन्तु इसमें बढ़ोतरी करने पर सरकारों ने अब तक कोई तवज्जो नहीं दी है।
यूँ तो लम्बे समय से कालाहाण्डी का नाम देश के सर्वाधिक पिछड़े ज़िले के रूप में शामिल रहा है, परन्तु अब यहाँ की फ़िज़ा काफी बदल चुकी है,आवश्यकता है तो बस उसे तराशने एवं सहेज कर रखने की। हाल ही के एक आंकलन में कालाहाण्डी को देश के अठारह महत्वाकांक्षी ज़िलों में से एक बतलाया गया है। जानकारी के मुताबिक़ ज़िले में केवल धान एवं कपास का ही सालाना उत्पादन कोई 16 करोड़ का होता है, जबकि फल एवं सब्जियों से भी कोई पांच करोड़ की आय होती है। सूचनानुसार इससे राज्य सरकार को भी 53 करोड़ का शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। यह सब प्रकृति प्रदत्त अथवा परम्परागत खेती से प्राप्त होता है, परन्तु इसमें बढ़ोतरी करने पर सरकारों ने अब तक कोई तवज्जो नहीं दी है।
विडम्बना की बात तो यह है कि इतनी अच्छी संभावनाओं के बावज़ूद आज़ादी के सात दशक बाद भी यहाँ कृषि आधारित कोई बड़ा कारख़ाना स्थापित नहीं किया गया है एवं रोज़गार की तलाश में सालाना कोई पचास हज़ार लोग अन्यत्र पलायन करने को विवश हैं। इस बात का एहसास वर्तमान में तब अधिक होता है, जब कोविड-19 के चलते बड़ी तादाद में लोग अन्य प्रदेशों से घर लौट रहे हैं। यह एक कड़वा सच है कि परम्परागत कृषि के इस गढ़ पर सरकारें कभी ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझतीं, जिसके चलते लोग बंधुआ मज़दूरी करने अन्य प्रदेशों का रुख करने को मज़बूर होते हैं।

गत 80 के दशक में यहाँ गुरबत की स्थिति ऐसी थी कि यह क्षेत्र भुखमरी के चलते बच्चों की बिक्री एवं आम की गुठली खाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सुर्ख़ियों में छाया हुआ था, परन्तु आज बहुमुखी इन्द्रावती परियोजना की बदौलत धान उत्पादन के लिये पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। कपास उत्पादन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है और यहाँ की कपास का रेशा भी काफी उन्नत मान का समझा जाता है।
कहने को ज़िले में उद्योगों की शुरुआत के तौर पर कोई तीन दशक पहले यहां एक कताई मिल का शिलान्यास कर उस पर इमारती ढ़ांचा भी खड़ा किया गया, जो कि अब खण्डहर में तब्दील हो चुका है। इस प्रकार योजना को एकाएक त्याग दिये जाने पर पन्द्रह करोड़ की लागत बेकार हो गयी।
प्रचुर मात्रा में धान उत्पादन के चलते यहाँ कोई साठ-सत्तर चावल मिलें तो हैं, परन्तु उससे जुड़े कोई सहयोगी उद्योग अथवा कृषि आधारित कोई अन्य बड़ा उद्योग नहीं है, जबकि उद्योग के लिये आवश्यक कच्चा माल, आधारभूत ढ़ांचा एवं कृषि महाविद्यालय जैसी सुविधाएं यहाँ मौज़ूद होने के बावज़ूद सरकारें ध्यान देना आवश्यक नहीं समझतीं।
वैसे भी यहाँ की अस्सी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है तथा धान और कपास के अलावा प्याज़, सब्जियां, आम, अनानास आदि का उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में होता है, परन्तु अफ़सोस कि तत्सम्बन्धी कोई उद्योग, प्रसंस्करण अथवा विपणन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उत्पादकों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां अकेले रबी एवं खरीफ़ ऋतु में सालाना कोई 70 लाख क्विंटल धान की पैदावार होती है, जिसकी क़ीमत 1270 करोड़ बैठती है, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। इतना ही नहीं सरकार धान की विपणनकारी नियंत्रित बाज़ार समिति तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी अतिरिक्त राजस्व हासिल करती है, लेकिन उक्त संस्थाएं किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम रही हैं। एक समय था, जब उक्त दोनों संस्थाएं रुग्णावस्था में थीं, फिर पड़ौसी राज्य छत्तीसगढ़ की तर्ज़ पर धान क्रय प्रणाली को अपना कर संस्थाओं द्वारा एक दशक की अवधि में किसानों की सहायता के नाम पर चार सौ करोड़ का राजस्व हासिल कर स्वयं को तो दुरुस्त कर लिया, परन्तु किसानों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की गयी।

ज़िले में स्थापित 60 चावल मिलें भी त्रुटिपूर्ण सरकारी नीतियों के चलते साल में कोई आठ महीने ही चल पाती हैं, जानकारों की मानें तो यदि छत्तीसगढ़ अथवा आंध्रप्रदेश की तरह सेलिंग एवं मिलिंग को नियंत्रण-मुक्त कर दिया जाये, तो मिलें न केवल पूरे साल चल सकती हैं, बल्कि बढ़ी चार महीने की अवधि में अतिरिक्त 36 सौ मज़दूरों को रोज़गार भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, धान के अपशिष्ट से धान की भूसी से निकलने वाले खाद्य तेल, मदिरा हेतु स्प्रिट, ईंधन के तौर पर इथोनॉल तथा मुर्गा एवं गोखाद्य आदि के कारखाने भी लगाये जा सकते हैं। लेकिन इस पर सरकारों की अब तक कोई सोच ही नहीं रही है। यदि सरकारी नीतियों में समुचित परिवर्तन किया जाये, तो न केवल धान-चावल उद्योग का आकार बढ़ा कर दुगुना किया जा सकता है, अपितु मज़दूरों के पलायन पर भी क़ाबू पाना सम्भव है।
यह आंकड़ा भी चौंकाने वाला है कि ज़िले में सालाना 6 लाख क्विंटल कपास उत्पादन और 330 करोड़ के कारोबार से सरकार को बज़रिये आरएमसी 6 करोड़ रुपये बतौर राजस्व प्राप्त होता है, इसके बावज़ूद केसिंगा स्थित ज़िले की एकमात्र कोणार्क स्पीनिंग मिल तीन दशक से अपने हाल पर आँसू बहा रही है। यहां की कपास की गुणवत्ता विश्वस्तरीय तथा उत्पादन इतना है कि जिससे एकसाथ चार बड़ी कताई मिलें चलाई जा सकती हैं। कपास उत्पादन के क्षेत्र में कालाहाण्डी पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। यहाँ कपास उत्पादन से संभावनाएं इतनी हैं कि वस्त्रोद्योग का एक पूरा हब विकसित किया जा सकता है और तब किसी श्रमिक को न तो मज़दूरी के लिये सूरत जाने की आवश्यकता होगी और न ही कोविड-19 का ख़तरा होगा। बल्कि प्रदेश के अन्य भागों के श्रमिकों की रोजीरोटी का जुगाड़ भी यहीं बन जाता।

चूंकि यहां कृषि महाविद्यालय भी स्थापित हो चुका है, अतः कृषि आधारित उद्योग लगने पर यहां से निकलने वाले छात्र-छात्राओं को भी उसका पूरा लाभ मिलेगा। यदि सरकारी इच्छाशक्ति हो, तो वह वर्तमान प्राप्त राजस्व से ही कताई मिल चालू कर सकती है।
विडम्बना की बात यह भी है कि यहाँ से भेजे गये कच्चे माल से अन्य प्रदेश तो मालामाल हो रहे हैं, परन्तु यहां की हालत पतली है। लापरवाही का आलम यह है कि यहां प्याज़ का भरपूर उत्पादन तो होता है, परन्तु उसे सुरक्षित रखने एक भी शीतलगृह नहीं है, जिसके चलते सीजन समाप्ति के बाद प्याज़ की किल्लत पैदा हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि जिस किसान को शुरुआत में महज़ चार-पांच रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है, बाद में वह उसे 30-35 रुपये के भाव ख़रीदने को मज़बूर होता है। नियमगिरि की पहाड़ियों में अनानास की उपज प्रचुर मात्रा में होती है, परन्तु प्रसंस्करण की सुविधा न होने के कारण आदिवासियों को उसकी क़ीमत महज़ 5-6 रुपये ही मिल पाती है। आम का उत्पादन भी क्षेत्र में काफी बढ़ा है और जो आम बैंगलुरु जैसे महानगर में डेढ़-दो सौ रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है, उसकी क़ीमत यहां बमुश्किल 15-20 रुपये ही मिल पाती है।
आइये जानें कि इस विषय पर अंचल के तमाम नेता एवं बुध्दिजीवी क्या राय रखते हैं।
 ओड़िशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रदीप्त कुमार नायक का कहना है कि -कालाहाण्डी की विश्वस्तरीय कपास के लिये स्पीनिंग सहित तमाम उद्योगों की ज़रूरत है, जिससे कोई पन्द्रह हज़ार रोज़गार के नये अवसर पैदा किये जा सकते हैं। इसी प्रकार धान एवं अन्य कृषि आधारित उद्योग खड़े किया जाना भी क्षेत्र के विकास हेतु अत्यावश्यक है। मैं इस प्रसंग को विधानसभा में उठाऊंगा एवं राज्य सरकार ने पहल की तो केन्द्र अवश्य मदद करेगा।
ओड़िशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रदीप्त कुमार नायक का कहना है कि -कालाहाण्डी की विश्वस्तरीय कपास के लिये स्पीनिंग सहित तमाम उद्योगों की ज़रूरत है, जिससे कोई पन्द्रह हज़ार रोज़गार के नये अवसर पैदा किये जा सकते हैं। इसी प्रकार धान एवं अन्य कृषि आधारित उद्योग खड़े किया जाना भी क्षेत्र के विकास हेतु अत्यावश्यक है। मैं इस प्रसंग को विधानसभा में उठाऊंगा एवं राज्य सरकार ने पहल की तो केन्द्र अवश्य मदद करेगा।
 ओड़िशा शासन में ऊर्ज़ा, एमएसएमई एवं गृहमंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र कहते हैं कि -प्रचुरता से परिपूर्ण कालाहाण्डी ने धान एवं कपास उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्तमान में प्रदेश सरकार की ज़िले में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना है, जिसके तहत तमाम विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर बाहरी उद्यमियों को आमंत्रित कर छोटे-छोटे कारख़ाने स्थापित किये जायेंगे। जिसमें सरकार का सम्पूर्ण सहयोग रहेगा। मुख्यमंत्री की ज़िले पर ख़ास ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ ऊर्ज़ा की कोई समस्या नहीं रहेगी, अतः उद्योगों में स्वाभाविक तौर पर लोगों की रुचि होगी। आंध्रप्रदेश की तरह यहां भी कुक्कुट, अंडा एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देकर लोगों को स्वावलंबी बनाया जायेगा।
ओड़िशा शासन में ऊर्ज़ा, एमएसएमई एवं गृहमंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र कहते हैं कि -प्रचुरता से परिपूर्ण कालाहाण्डी ने धान एवं कपास उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्तमान में प्रदेश सरकार की ज़िले में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना है, जिसके तहत तमाम विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर बाहरी उद्यमियों को आमंत्रित कर छोटे-छोटे कारख़ाने स्थापित किये जायेंगे। जिसमें सरकार का सम्पूर्ण सहयोग रहेगा। मुख्यमंत्री की ज़िले पर ख़ास ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ ऊर्ज़ा की कोई समस्या नहीं रहेगी, अतः उद्योगों में स्वाभाविक तौर पर लोगों की रुचि होगी। आंध्रप्रदेश की तरह यहां भी कुक्कुट, अंडा एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देकर लोगों को स्वावलंबी बनाया जायेगा।
 राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार भी ज़िले में कृषि आधारित उद्योगों की भारी संभावना देखते हुये कहते हैं कि -टेक्सटाइल पार्क एवं कोणार्क स्पीनिंग मिल को शुरू करने के अलावा उससे जुड़ी इकाइयों पर भी सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद ज़िले का विकास अवश्य होगा।
राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार भी ज़िले में कृषि आधारित उद्योगों की भारी संभावना देखते हुये कहते हैं कि -टेक्सटाइल पार्क एवं कोणार्क स्पीनिंग मिल को शुरू करने के अलावा उससे जुड़ी इकाइयों पर भी सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद ज़िले का विकास अवश्य होगा।
 पूर्व केन्द्रीय मंत्री भक्तचरण दास भी कृषि आधारित उद्योगों के लिये यहाँ माहौल माक़ूल मानते हैं, फिर चाहे बात नियमगिरि के अनानास या आमों की हो या कि धान, मकई, कपास अथवा प्याज़ उत्पादन की, तत्सम्बन्धी इकाइयों की यहाँ सख़्त ज़रूरत है। जिससे रोज़गार के अवसर अवश्य बढ़ेंगे एवं खुशहाली आयेगी। आवश्यकता है तो बस, राज्य एवं केन्द्र सरकार की आन्तरिकता तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रयासों की। इस पर कोई प्रयास नहीं हो रहा, जिसके चलते यहाँ मांडिया, रागी, खोसला, गुर्जी आदि की उपज में काफी गिरावट आयी है।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री भक्तचरण दास भी कृषि आधारित उद्योगों के लिये यहाँ माहौल माक़ूल मानते हैं, फिर चाहे बात नियमगिरि के अनानास या आमों की हो या कि धान, मकई, कपास अथवा प्याज़ उत्पादन की, तत्सम्बन्धी इकाइयों की यहाँ सख़्त ज़रूरत है। जिससे रोज़गार के अवसर अवश्य बढ़ेंगे एवं खुशहाली आयेगी। आवश्यकता है तो बस, राज्य एवं केन्द्र सरकार की आन्तरिकता तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रयासों की। इस पर कोई प्रयास नहीं हो रहा, जिसके चलते यहाँ मांडिया, रागी, खोसला, गुर्जी आदि की उपज में काफी गिरावट आयी है।
 बुध्दिजीवी अक्षय नंद भी कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं देखते हुये कहते हैं कि -इसके लिये निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा सरकार की आन्तरिकता का स्पष्ट अभाव है। कताई मिल से लेकर चावल मिल से जुड़ी सहयोगी इकाइयों तक के लिये तमाम ढांचागत सुविधाएं यहाँ मौज़ूद हैं, कमी है तो बस प्रयासों और इच्छाशक्ति की। उन्होंने कहा -ज़िले के पर्वतीय क्षेत्र में औषधीय वनस्पतियों का भी भण्डार है, अतः जिनके दोहन से यहां दवा उद्योग को भी विकसित किया जा सकता है। यहां के कच्चे माल के सहारे अन्य राज्यों के उद्योग फ़लफूल रहे हैं, जबकि यहां सब कुछ होते हुये भी कुछ नहीं है। यह तो ज़िले के साथ घोर अन्याय है।
बुध्दिजीवी अक्षय नंद भी कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं देखते हुये कहते हैं कि -इसके लिये निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा सरकार की आन्तरिकता का स्पष्ट अभाव है। कताई मिल से लेकर चावल मिल से जुड़ी सहयोगी इकाइयों तक के लिये तमाम ढांचागत सुविधाएं यहाँ मौज़ूद हैं, कमी है तो बस प्रयासों और इच्छाशक्ति की। उन्होंने कहा -ज़िले के पर्वतीय क्षेत्र में औषधीय वनस्पतियों का भी भण्डार है, अतः जिनके दोहन से यहां दवा उद्योग को भी विकसित किया जा सकता है। यहां के कच्चे माल के सहारे अन्य राज्यों के उद्योग फ़लफूल रहे हैं, जबकि यहां सब कुछ होते हुये भी कुछ नहीं है। यह तो ज़िले के साथ घोर अन्याय है।







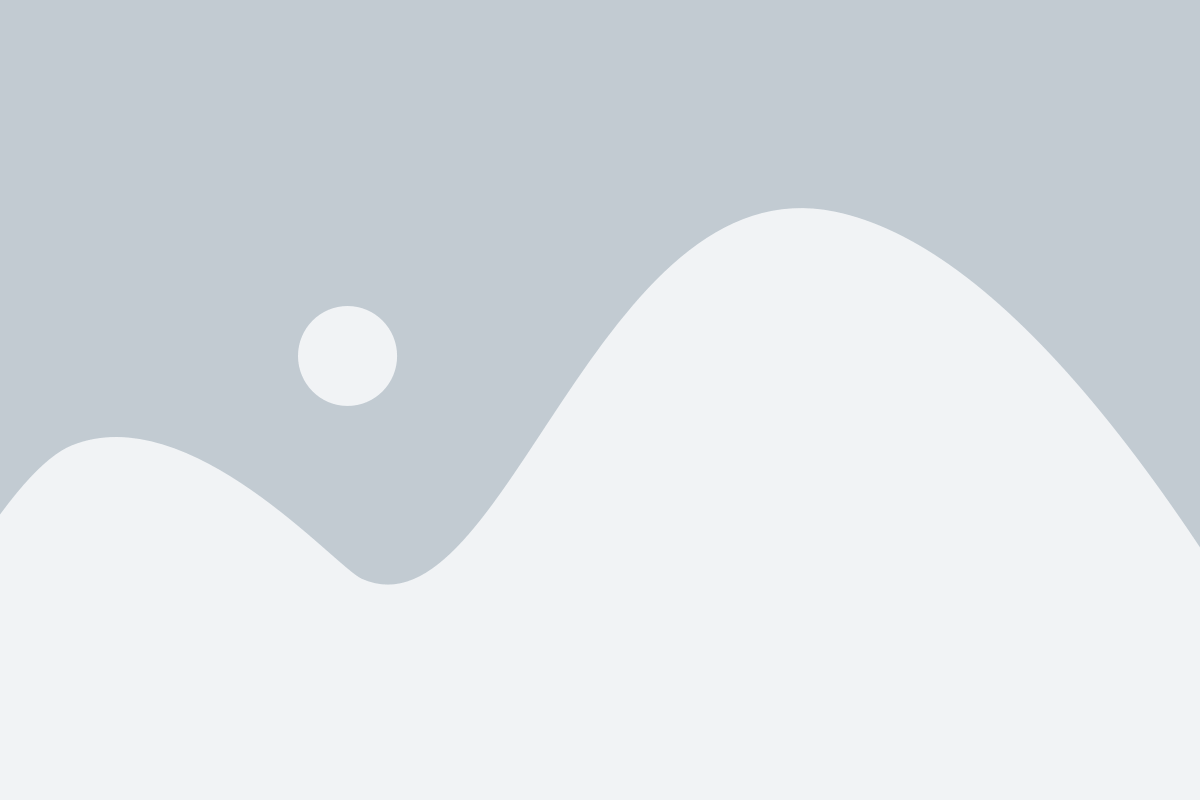
Leave a Comment